असभ्य, असामाजिक बनाने की परियोजना का हिस्सा है भाषा का क्षरण
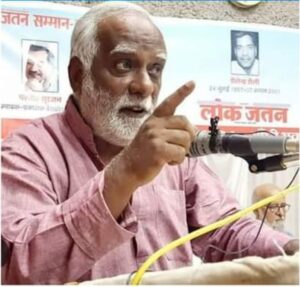
बादल सरोज
इस कालखंड के बारे में जो बात एकदम पक्की है, वह यह है कि इसे नैतिकता, शुचिता, सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार के पतन, वायदों और घोषणाओं के प्रति निर्लज्जता की सारी हदें पार करने वाली बेशर्मी के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। इतिहास में यह समय सत्य के देश निकाले और झूठ के राज्यारोहण के दुस्समय के रूप में दर्ज किया जाएगा।
जिस निर्लज्ज दीदादिलेरी के साथ सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग, जिनमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, बिना पलक झपकाए झूठे वादे और निराधार दावे कर रहे हैं, वह चौकाने वाला घटनाविकास है। ऐसी घोषणाएं की जा रही है, जिन्हें पिछले कई वर्षों से बार-बार करके चुनाव जीते गए, मगर वे कहीं भी पूरी नहीं की गयीं। ऐसे दावे किये जा रहे हैं, जिनका न कोई तर्क है, न आधार है, बल्कि ज्यादातर के मामले में तो सच्चाई उससे ठीक उलट है।
जाहिर है कि इतना जबर आत्मविश्वास यूं ही नहीं आ जाता : इसके पीछे पाल-पोसकर वर्चस्व बनाकर मीडिया में बिठाए गए अपने ढिंढोरचियों के वृन्दगान की कारगरता पर यकीन होता है। यह भरोसा होता है कि जब तक तथ्यों सहित सच अपने जूतों के फीते बांधेगा, तब तक इनका झूठ आधी दुनिया में अपना झंडा लहरा चुका होगा।
ऐसा रातों-रात नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत पूंजीवादी समाज के – भले दिखावटी ही सही – सामाजिक व्यवहार के शिष्टाचार को गहरे में दफनाने से हुयी। भारत की सामाजिक-राजनीतिक विरासत के प्रतीक, स्वतन्त्रता संग्राम के आइकॉन रहे नायकों के बारे में ऊलजलूल बातों से शुरू हुआ सिलसिला उनके बारे में गढ़े गए झूठों के अभद्र और अश्लीलता की सीमाएं पार करने वाले धुंआधार हमलों तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति तक ने ‘हम 5 हमारे 125’ ‘पचास करोड़ की गर्ल फ्रेंड’ से लेकर ‘कांग्रेस की विधवा’ जैसे शब्द-युग्मों से आरम्भ करके उसे ‘मारब सिक्सर से छह गोली छाती में’ तक की ऊंचाई तक पहुंचाया।
यह शीर्ष की निम्नता थी, नीचे के कुनबे में यह और कितने नीचे तक पहुंची, इसे जानने के लिए गिरिराज सिंह और हिमंता विश्वसरमा के आप्त वचन देखे जा सकते हैं। भाषा का यह क्षरण चौंकाने वाला है। इस अमर्यादित, अशिष्ट भाषा को सड़क छाप कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा, इसे कम करके देखना होगा। यह समाज को अराजक और उसमे रहने वालों को वहशी बनाने की महापरियोजना का एक हिस्सा भर है। इसी के साथ यह भी कि भाषा के इस पतन को सिर्फ भाषा से जोड़कर देखना ठीये तक नहीं पहुंचाएगा। इसे उसकी समग्रता में देखना होगा।
भाषा और वर्तनी सिर्फ संवाद या संचार का माध्यम नहीं होती। हमारे समय के सबसे बड़े भाषा विज्ञानी नोम चोम्स्की मीडिया और राजनीतिक प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का विश्लेषण करते हुए ठीक ही बताते हैं कि सत्ता में बैठे लोग जनमत को अपने अनुकूल ढालने, अपनी आमतौर से अस्वीकार्य विचारधारा को जनता के गले उतारने और उसे फैलाने के साथ-साथ सामाजिक गैरबराबरी को मजबूत करने के लिए भाषा का उपयोग एक औजार के रूप में करते हैं।
चोम्स्की भाषा की सार्वभौमिकता पर जोर देते हुए उसका उपयोग आमतौर से शक्ति के खेल का एक हिस्सा बताते हैं। वे बताते हैं कि मीडिया और प्रचार किस तरह भाषा का उपयोग करके लोगों की धारणाओं को नियंत्रित करते हैं। सहमति का उत्पादन – कंसेंट को मैन्युफेक्चर – करते है। गरज यह कि इस तरह से जनता को उन बातों के लिए राजी किया जाता है, जो दरअसल खुद उसके हितों के ही खिलाफ होती हैं। इन दिनों इस सबको होता हुआ देखा जा सकता है। इस तरह से भाषा वैचारिक प्रभुत्व कायम करने का एक माध्यम बन जाती है, जहाँ हुक्मरानों के जनविरोधी, समाजविरोधी विचार स्वाभाविक, सहज और सामान्य विचारों के रूप में प्रस्तुत किए जाने लगते हैं, नियति और अपरिहार्य बताये जाते हैं, वहीँ जनहितैषी वैकल्पिक विचारों को हाशिये पर धकेल दिया जाता है।
इस तरह वर्ग विभाजित समाज में भाषा शक्ति की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्चस्व और नियंत्रण का एक सूक्ष्म, लेकिन शक्तिशाली जरिया बन जाती है। नवउदार के दौर में भाषा ने इस तरह की भूमिका पूरे प्राण-प्रण से निबाही। शब्दों को नए और एकदम उलट अर्थ दे दिए गए। दिखने-सुनने में आकर्षक, किन्तु सीधे काशी करवट करवाने वाले शब्द गढ़ लिए गए, जिनमें भूख को तप और मृत्यु को मोक्ष के रूप में महिमामंडित कर दिया गया।
मोदी राज में यह गिरावट भयानक गति के साथ हुयी और लगातार जारी है। एक समय था, जब पूंजीवादी लोकतंत्र, उसमें भी संसदीय लोकतंत्र, कम-से-कम अपने वर्ग के विरोधियों के प्रति बर्ताब के मामले में एक दायरे में रहता था। एक दूसरे के प्रति – भले दिखावे के लिए ही – संयमित और सभ्रांत वर्तनी के लिए जाना जाता था। राजनीतिक विपक्ष विरोधी होता था, दुश्मन नहीं। कहे-लिखे की जांच, समीक्षा और उसकी प्रामाणिकता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। असत्य को ज्यादा दिनों तक तथ्य बनाकर प्रस्तुत नही किया जा सकता था। झूठ के कोलाहल की आयु अधिक नहीं हुआ करती थी। मगर जैसे-जैसे पांवों के नीचे से जमीन खिसकती गयी, वैसे-वैसे मुखौटे सरकते और उतरते गए। सिर्फ भाषा ही पतित नहीं हुई, प्रस्तुति भी विकृत होती गयी।
मोदी राज में इसे बाकायदा कोरियोग्राफ करके ढाला गया है : नथुने फुलाकर, कर्कश और चीख-चिल्लाकर बोलना, भुजाएं फड़काना, शोर मचाना, अश्लीलता की हद तक भद्दे और भौंडे इशारे करना, यह सब करने के लिए संसद तक के मंच का उपयोग करना, आम बात बन गयी। मौजूदा सत्ता पार्टी के खुद के हिसाब से भी यह नीचाई नयी बात है। इससे पहले भले निबाहा न जाता हो, मगर राजधर्म का हवाला तो देना ही पड़ता था : अब यह सब पुरानी बातें हो गयीं है। झूठ गालियों और धमकियों के पारदर्शी पैरहन में नंगा घूम रहा है।
यह सिर्फ किसी व्यक्ति तक महदूद विकार नहीं है, यह विचार का व्यवहार है। भाषाविद कहते हैं कि भाषा हमारा स्वयं का परिचय होती है। बोलने वालों के चरित्र और विकास का सटीक प्रतिबिंब होती है। इसी के साथ भाषा किसी संस्कृति का रोडमैप होती है, जो यह बताती है कि इसके लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस हिसाब से मोदी और उनके अमित शाह सहित बाकी सब उनके अपनों की भाषा एकदम उनके चरित्र और विकास पर फिट बैठती है।
गरल किसी भी रूप या आकार में निकले, वह दूध या अमृत नहीं बनेगा, गरल ही रहेगा। यह वही नफरती विष है, जिसके प्रवाह और आचमन में यह कुनबा सिद्ध है, यह वही रोडमैप है, जिस पर यह देश को रसातल में ले जाना चाहता है । दोबारा से एक ऐसे समाज में पहुंचाना चाहता है, जहां भाषा स्त्रियों और दलितों की गरिमा और मनुष्यता को छीनने के हथियार की तरह उपयोग में लायी जाती रही। जहां राज करने वालों की भाषा को देवत्व प्रदान कर दिया गया और बाकियों के लिए उसके इस्तेमाल तक पर रोक लगा दी गयी। साहित्य और नाटकों तक में उनके हिस्से आये संवाद उन्हीं भाषाओं में लिखे गए, जिन्हें हीन माना गया था। यह अलग बात है कि ऐसा करने वाले यह भूल गए कि अंततः यह उन्हें भी नहीं बख्शेगा ; लौट-फिरकर उन्हीं पर आयेगा। वही तब भी हुआ, आज भी हो रहा है। वह कथित देवभाषा ही लुप्त होने की कगार पर पहुँच गयी।
2014 के बाद सबसे ज्यादा अवमूल्यन भाषा का हुआ है। किसी भी दिन, किसी भी विषय पर, कोई भी कथन देखें, उसमें बड़बोलापन और खोखलापन एक साथ दिखाई देता है। भाषा में छल-कपट और सतहीपन आया है और वह अपनी पिछली ताकत खो बैठी है। इसकी एवज में उसने जिस शक्ति को पाया है, वह नकारात्मक ऊर्जा की ज्वाला है।
भाषा दोधारी तलवार की तरह होती है। माना यह जाता है कि हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैँ, मगर अक्सर, और वर्ग समाज में ख़ासकर, भाषा भी हमारा इस्तेमाल करती है। समाज की परम्पराओं और विरासतों के साथ खिलवाड़ अपनों को भी नहीं छोड़ता। झुलसन ज्वाला भड़काने वालो को भी अपनी चपेट में लेती हैं। अडवानी और गोविन्दाचार्य, कल्याण सिंह और उमा भारती इसे भुगत चुके हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं और कल नही होंगे, तब उनके हिस्से भी यही आना है। चिंता उनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, की नहीं है, फ़िक्र इस बात की है कि इस सबके चलते पूरे समाज की वर्तनी में, फिलहाल अपरिवर्तनीय दिखता जो परिवर्तन हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई और दुरुस्ती में कितना वक़्त लगेगा।
इसलिए कि यह सिर्फ संबोधन ही विकृत नहीं कर रही है, राजनीति ही नहीं, सामाजिक बर्ताव से सामूहिकता भी छीन रही। लोकतंत्र में जिस ‘हम’ का होना पहली शर्त हुआ करती थी, वह व्यक्ति के अहम में रूपांतरित होते होते ‘मै’ ‘मैं’ के आत्मालाप में प्राणप्रतिष्ठित हो चुकी है। सिर्फ मोदी और उनके कुनबे की ही नहीं, ज्यादातर विपक्ष का लहजा बन चुकी है। यह सिर्फ व्याकरण का मसला नहीं है – यह आचरण का मामला है, जो संसदीय लोकतंत्र में उस व्यक्ति केन्द्रिकता को स्थापित करता है, जिसमे तानाशाही और अधिनायकत्व के खतरे निहित हैं।
यह सब अनायास नहीं है, यह सोचे-समझे तरीके से तैयार किया गया रोडमैप है। यह लोगों के लिए खुद को बदलने की बजाय अपने अनुकूल लोग तैयार करने की कोशिश का हिस्सा है। समाज को सामाजिकता के सहज गुण से वंचित करने की परियोजना है। इसलिए इसे महज कुछ व्यक्तियों का मुखालाप मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसे सहेजने और बचाने का काम भी किसी और के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता।
(लेखक ‘लोकजतन’ के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 9425006716)


