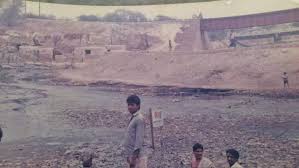[जलवायु शरणार्थी: जिनके आँकड़े हैं, पर जिनकी आवाज़ नहीं]
पानी जब अपनी सीमा लांघता है, तो न मानचित्र की रेखाओं को पहचानता है, न दीवारों को, न सरहदों को।और जब धरती की छाती फटती है, तो वह खेत, घर और जीवन सबको निगल लेती है। यही जलवायु संकट है, जिसके सामने आज दुनिया खड़ी है। यह संकट केवल ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के बढ़ने या तापमान के उबलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल की ओर इशारा करता है—जब गाँव डूबेंगे, जब शहर सूखेंगे, जब खेत बंजर होंगे, तब करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे? वे कहाँ अपना घर बनाएंगे, और क्या उन्हें कहीं जगह मिलेगी? यह सवाल न केवल पर्यावरण का है, बल्कि मानवता, नैतिकता और सामाजिक न्याय का है। यह उन करोड़ों लोगों की पुकार है, जो जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं, और जिनके पास न संसाधन हैं, न आवाज़, और न ही कोई ठौर।
विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। यह संख्या आज के कुल शरणार्थियों की संख्या से कई गुना अधिक है।ये लोग युद्ध या हिंसा के कारण नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज—बढ़ते समुद्र, भीषण सूखा, बेमौसम बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं के कारण उजड़ेंगे। भारत जैसे देश में यह संकट और भी गहरा है, जहाँ 1.4 अरब की आबादी का बड़ा हिस्सा तटीय इलाकों, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों और सूखाग्रस्त मैदानों में रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आँकड़े बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में भारत में चक्रवातों की तीव्रता में 20% की वृद्धि हुई है, और सूखे की घटनाएँ भी दोगुनी हो गई हैं। सुंदरबन, जो पहले से ही समुद्र के बढ़ते स्तर से जूझ रहा है, वहाँ हर साल हज़ारों लोग अपनी ज़मीन खो रहे हैं। असम में बाढ़ अब सालाना त्रासदी बन चुकी है, जिसने 2022 में 55 लाख लोगों को प्रभावित किया। बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सूखे ने लाखों किसानों को खेती छोड़ने और शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया है।
इस संकट की एक और विडंबना यह है कि जलवायु शरणार्थियों को अभी तक अंतरराष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं मिली है। 1951 का जेनेवा शरणार्थी सम्मेलन केवल उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा देता है जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने देश छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई बाढ़, सूखा या तूफान के कारण बेघर हो जाए, तो वह इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता।इसका मतलब है कि जलवायु शरणार्थियों को न तो अपने देश में और न ही विदेश में कोई कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह एक गहरी खामी है, जो दुनिया के नीति-निर्माताओं की उदासीनता को दर्शाती है। कुछ देशों, जैसे न्यूज़ीलैंड और स्वीडन, ने इस दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अभी तक कोई ठोस ढांचा नहीं बना।
भारत में स्थिति और भी जटिल है। यहाँ पहले से ही आंतरिक विस्थापन एक बड़ी समस्या है।2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 1.4 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होते हैं। यह संख्या किसी भी युद्धग्रस्त देश से कहीं अधिक है। और जब ये लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो वे पहले से ही तनावग्रस्त शहरी ढांचे पर बोझ बन जाते हैं। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और इनमें से अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं। लेकिन सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ इन्हें शरणार्थी के रूप में नहीं देखतीं; ये लोग केवल प्रवासी कहलाते हैं, और उनकी कहानियाँ आधिकारिक दस्तावेज़ों में गुम हो जाती हैं।
इस संकट की जड़ें गहरी हैं और केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं हैं।हमारा विकास मॉडल, जो मुनाफ़े और अनियंत्रित शहरीकरण पर आधारित है, इस समस्या को और बढ़ा रहा है। हमने जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया, और जल प्रबंधन को बाज़ार के हवाले कर दिया। भारत में भूजल स्तर पिछले 30 वर्षों में 20% तक गिर चुका है, और अनुमान है कि 2030 तक देश के कई हिस्सों में पानी की भयंकर कमी होगी। साथ ही, हमारी कृषि नीतियों ने छोटे किसानों को कर्ज और निर्भरता के जाल में फँसाया, जिससे वे जलवायु परिवर्तन की मार को झेलने में और कमज़ोर हो गए।
इस संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह असमानता को और गहरा करता है। गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाएँ और बच्चे—ये वे लोग हैं जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक अमीर व्यक्ति हमेशा बेहतर जगह पर जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही हाशिए पर हैं, उनके लिए कोई ठौर नहीं है। उदाहरण के लिए, सुंदरबन में रहने वाली आदिवासी महिलाएँ, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अब समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अपनी आजीविका और सुरक्षा खो रही हैं। यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है; यह सामाजिक न्याय का सवाल है।
क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, लेकिन इसके लिए साहस, दूरदृष्टि और सामूहिक इच्छाशक्ति चाहिए। सबसे पहले, हमें जलवायु शरणार्थियों को एक मानवाधिकार के रूप में देखना होगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाना होगा, जो इन लोगों को सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दे। दूसरा, हमें अपने शहरों को इस तरह से पुनर्गठित करना होगा कि वे विस्थापित आबादी को समायोजित कर सकें। सस्ते आवास, रोज़गार के अवसर, और बुनियादी सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा इस दिशा में अनिवार्य हैं। तीसरा, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास पर ध्यान देना होगा—जल संरक्षण, जैविक खेती, और स्थानीय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण लोगों को उनके गाँवों में टिकाए रख सकता है।
सबसे ज़रूरी है वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय की माँग। विकसित देश, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन के ज़रिए इस संकट को जन्म दिया, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दें। पेरिस समझौते में 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता थी, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा ही अब तक दिया गया है। यह असमानता तब तक बनी रहेगी, जब तक अमीर देश अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते।
जलवायु शरणार्थियों की त्रासदी केवल आँकड़ों की नहीं है; यह हमारी साझा मानवता का सवाल है। जब समुद्र गाँवों को निगल रहा हो, जब धरती खेतों को बंजर बना रही हो, तब हमारी चुप्पी और निष्क्रियता हमें भी इस संकट का हिस्सा बनाती है। यह समय है कि हम न केवल अपने घरों को बचाएँ, बल्कि उस धरती को भी बचाएँ जो हम सबका घर है। अगर हम अभी नहीं जागे, तो वह दिन दूर नहीं जब लाखों लोग हमारे दरवाज़े पर खड़े होंगे, और हमसे पूछेंगे—“अब हम कहाँ जाएँ?” क्या हमारे पास तब कोई जवाब होगा?

प्रो. आरके जैन “अरिजीत